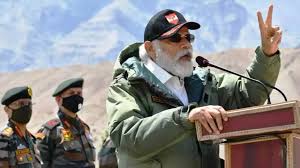-ललित गर्ग-
-: ऐजेंसी सक्षम भारत :-
कुपोषण और भुखमरी से जुड़ी ताजा रिपोर्ट न केवल चैंकाने बल्कि सरकारों की नाकामी को उजागर करने वाली है। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि एक ओर विकास और अर्थव्यवस्था की भावी सुखद तस्वीर की चमक की बात की जा रही हो और दूसरी ओर देश में बच्चों के बीच कुपोषण की समस्या के गहराते जाने के आंकड़े सामने आएं। जबकि अमूमन हर कुछ रोज बाद इस तरह की बातें शीर्ष स्तर से कही जाती रहती हैं कि बच्चे चूंकि भविष्य की उम्मीद और बुनियाद हैं, इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने सहित बाकी मामलों में भी उनके जीवन-स्तर में बेहतरी जरूरी है। लेकिन ताजा कुपोषण एवं भुखमरी के आंकड़े शासन-व्यवस्था की एक शर्मनाक विवशता है। लेकिन इस विवशता को कब तक ढोते रहेंगे और कब तक देश में कुपोषितों का आंकड़ा बढ़ता रहेगा, यह गंभीर एवं चिन्ताजनक स्थिति है। लेकिन ज्यादा चिंताजनक यह है कि तमाम कोशिशों और दावों के बावजूद कुपोषितों और भुखमरी का सामना करने वालों का आंकड़ा पिछली बार के मुकाबले हर बार बढ़ा हुआ ही निकलता है।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार देश में तैंतीस लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं। इनमें से आधे से अधिक बच्चे अत्यंत कुपोषित की श्रेणी में आते हैं। ये आंकड़े पिछले साल विकसित पोषण ऐप पर पंजीकृत किए गए, ताकि पोषण के नतीजों पर निगरानी रखी जा सके। फिलहाल आंगनवाड़ी व्यवस्था में शामिल करीब 8.19 करोड़ बच्चों में से चार फीसद से ज्यादा बच्चों को कुपोषित के दायरे में दर्ज किया गया है। लेकिन न सिर्फ यह संख्या अपने आप में चिंताजनक है, बल्कि इससे ज्यादा गंभीर पक्ष यह है कि पिछले साल नवंबर की तुलना में इस साल अक्तूबर में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की तादाद में इक्यानबे फीसदी की बढ़ोतरी हो गई है। विचित्र यह भी है कि बच्चों के बीच कुपोषण की समस्या जिन राज्यों में सबसे ज्यादा है, उनमें शीर्ष पर महाराष्ट्र है। दूसरे स्थान पर बिहार और तीसरे पर गुजरात है। बाकी राज्यों में भी स्थिति परेशान करने वाली है, मगर यह हैरानी की बात है कि बिहार के मुकाबले महाराष्ट्र और गुजरात जैसे विकसित राज्यों में संसाधन और व्यवस्था की स्थिति ठीक होने के बावजूद बच्चों के बीच कुपोषण चिंताजनक स्तर पर है।
एक अन्य अध्ययन में कहा गया है कि भुखमरी एवं कुपोषण के खिलाफ दशकों से हुई प्रगति कोरोना महामारी की वजह से प्रभावित हुई है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा भारत सहित पूरे विश्व में भूख, कुपोषण एवं बाल स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त की गई है। यह चिन्ताजनक स्थिति विश्व का कड़वा सच है लेकिन एक शर्मनाक सच भी है और इस शर्म से उबरना जरूरी है। रिपोर्टें बताती हैं कि ऐसी गंभीर समस्याओं से लड़ते हुए हम कहां से कहां पहुंचे है। इसी में एक बड़ा सवाल यह भी निकलता है कि जिन लक्ष्यों को लेकर दुनिया के देश सामूहिक तौर पर या अपने प्रयासों के दावे करते रहे, उनकी कामयाबी कितनी नगण्य एवं निराशाजनक है।
यह सवाल तो उठता ही रहेगा कि इन समस्याओं से जूझने वाले देश आखिर क्यों नहीं इनसे निपट पा रहे हैं? इसका एक बड़ा कारण आबादी का बढ़ना भी है। गरीब के संतान ज्यादा होती है क्योंकि कुपोषण में आबादी ज्यादा बढ़ती है। विकसित राष्ट्रों में आबादी की बढ़त का अनुपात कम है, अविकसित और निर्धन राष्ट्रों की आबादी की बढ़त का अनुपात ज्यादा है। भुखमरी पर स्टैंडिंग टुगेदर फॉर न्यूट्रीशन कंसोर्टियम ने आर्थिक और पोषण डाटा इकट्ठा किया, इस शोध का नेतृत्व करने वाले सासकिया ओसनदार्प अनुमान लगाते हैं कि जो महिलाएं अभी गर्भवती हैं वो ऐसे बच्चों को जन्म देंगी जो जन्म के पहले से ही कुपोषित हैं और ये बच्चे शुरू से ही कुपोषण के शिकार रहेंगे। एक पूरी पीढ़ी दांव पर है।’
हालत यह है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत एक सौ एक वें स्थान पर जा चुका है। ऐसे में यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह तमाम बाधाओं के बीच अनिवार्य कार्यक्रमों को कैसे सुचारू रूप से संचालित करती है। वरना मौजूदा निराशाजनक तस्वीर के रहते हम किस कसौटी पर विश्व में एक बड़ी शक्ति होने का दावा कर सकेंगे? यह ध्यान रखने की जरूरत है कि कुपोषित बच्चों की मौजूदा समस्या विकास के दावों के सामने आईना बन कर खड़ी रहेगी। दरअसल, इस मसले पर हालात पहले ही संतोषजनक नहीं थे, लेकिन बीते एक साल के दौरान बच्चों के बीच कुपोषण की समस्या ने तेजी से अपने पांव फैलाए हैं। यह स्थिति तब है जब देश में एकीकृत बाल विकास जैसी महत्त्वाकांक्षी योजना से लेकर स्कूलों में मध्याह्न भोजन जैसे अन्य कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हालांकि बीते डेढ़ साल से ज्यादा समय से कोरोना महामारी की रोकथाम के क्रम में कई योजनाओं पर अमल में बाधाएं आई हैं। पूर्णबंदी के दौर में पहले ही करोड़ों लोग रोजी-रोजगार से वंचित हुए और इससे उनके खानपान और पोषण पर गहरा असर पड़ा।
महामारी के डेढ़ साल में कुपोषण के मोर्चे पर हालात और दयनीय हुए हैं। अब इस संकट से निपटने की चुनौती और बड़ी हो गई है। सत्ताएं ठान लें तो हर नागरिक को पौष्टिक भोजन देना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बाधा शासन-व्यवस्थाओं में बढ़ता भ्रष्टाचार है। गलत जब गलत न लगे तो यह मानना चाहिए कि बीमारी गंभीर है। बीमार व्यवस्था से स्वस्थ शासन की उम्मीद कैसे संभव है? आर्थिक सुधारों के क्रियान्वयन के लगभग 30 वर्षों के बाद असमानता, भूख और कुपोषण की दर में वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि समृद्धि के कुछ टापू भी अवश्य निर्मित हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोविड-19 के असर से पैदा हो रहे आर्थिक एवं सामाजिक तनावों पर विस्तृत जानकारी हासिल की है। भारत को लेकर प्रकाशित आंकड़े चिंताजनक हैं। एक तरफ हम खाद्यान्न के मामले में न केवल आत्मनिर्भर हैं, बल्कि अनाज का एक बड़ा हिस्सा निर्यात करते हैं। वहीं दूसरी ओर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कुपोषित आबादी भारत में है। भारत में महिलाओं की पचास फीसदी से अधिक आबादी एनीमिया यानी खून की कमी से पीड़ित है। इसलिए ऐसे हालात में जन्म लेने वाले बच्चों का कम वजन होना लाजिमी है।
राइट टु फूड कैंपेन नामक संस्था का विश्लेषण है कि पोषण गुणवत्ता में काफी कमी आई है और लॉकडाउन से पहले की तुलना में भोजन की मात्रा भी घट गई है। सवाल है कि अगर बच्चों में कुपोषण की समस्या चिंताजनक स्तर पर बरकरार रही तो विकास और बदलाव के तमाम दावों के बीच हम कैसे भविष्य की उम्मीद कर रहे हैं? भारत के साथ एक और विडम्बना है कि यहां एक तरफ विवाह-शादियों, पर्व-त्यौहारों एवं पारिवारिक आयोजनों में भोजन की बर्बादी बढ़ती जा रही है, तो दूसरी ओर भूखे लोगों के द्वारा भोजन की लूटपाट देखने को मिल रही है। भोजन की लूटपाट जहां मानवीय त्रासदी है, वहीं भोजन की बर्बादी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। एक तरफ करोड़ों लोग दाने-दाने को मोहताज हैं, कुपोषण के शिकार हैं, वहीं रोज लाखों टन भोजन की बर्बादी एक विडम्बना है। एक आदर्श समाज रचना की प्रथम आवश्यकता है अमीरी-गरीबी के बीच का फासला खत्म हो। खाने की बर्बादी रोकने की दिशा में ‘निज पर शासन, फिर अनुशासन’ एवं ‘संयम ही जीवन है’ जैसे उद्घोष को जीवनशैली से जोड़ना होगा। इन दिनों मारवाड़ी समाज में फिजूलखर्ची, वैभव प्रदर्शन एवं दिखावे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने एवं भोजन के आइटमों को सीमित करने के लिये आन्दोलन चल रहे हैं, जिनका भोजन की बर्बादी को रोकने में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। सरकार को भी शादियों में मेहमानों की संख्या के साथ ही परोसे जाने वाले व्यंजनों की संख्या सीमित करने पर विचार करना चाहिए। दिखावा, प्रदर्शन और फिजूलखर्च पर प्रतिबंध की दृष्टि से विवाह समारोह अधिनियम, 2006 हमारे यहां बना हुआ है, लेकिन यह सख्ती से लागू नहीं होता, जिसे सख्ती से लागू करने की जरूरत है। धर्मगुरुओं व स्वयंसेवी संगठनों को भी इस दिशा में पहल करनी चाहिए।