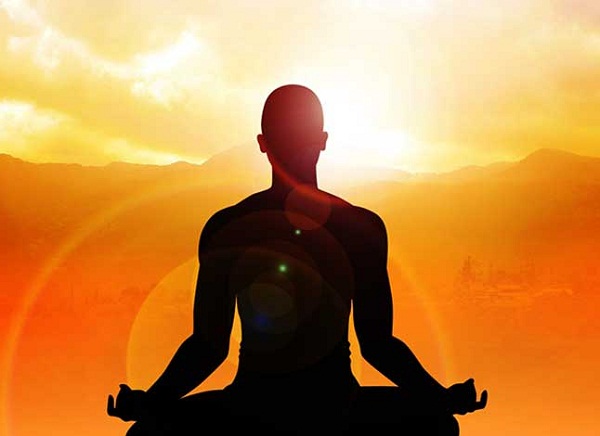
-हृदयनारायण दीक्षित-
-: ऐजेंसी सक्षम भारत :-
मन सभी ज्ञात वस्तुओं से ज्यादा गतिशील है। हमारा मन प्रायः वहाँ नहीं होता जहाँ हम होते हैं। हम घर में बैठे हैं। हमारा मन मथुरा और काशी में है। हम तीर्थाटन या पर्यटन की दृष्टि से किसी तीर्थ पर बैठे हैं। मन तीर्थों पर नहीं होता। घर चला जाता है। मन को समझने के गंभीर प्रयास हुए हैं। मन की प्रकृति को समझने के लिए पतंजलि ने बड़ा श्रम किया है। उन्होंने योग सूत्रों में (श्लोक-2) योग की परिभाषा की और कहा चित्तवृत्ति का निरोध योग है। उन्होंने चित्त की वृत्तियाँ भी बताई। मन की चर्चा ऋग्वेद में भी है।
यूरोप के विद्वानों ने मन पर पूरा विज्ञान ही खड़ा कर दिया है। वे उसे अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। मनोविज्ञानी सिग्मंड फ्रायड ने साइको एनालिसिस नाम की सुन्दर पुस्तक लिखी है। उनके समर्थक एडलर युंग ने भी साइको एनालिसिस या मन का विवेचन किया है। मन से तरंगें निकलती हैं। हम ऐसी तरंगों को मनतरंग कह सकते हैं। यजुर्वेद के 6 मन्त्र शिव संकल्प सूक्त कहे जाते हैं। इसके रचनाकार मन की चंचलता से परिचित थे। छहों मंत्र बड़े प्यारे हैं। ऋषि कहते हैं कि हमारा मन यहाँ-वहाँ बहुत दूर आकाश पर्वतों की ओर चला गया है, ”हे देवताओं हमारे मन को यहीं लौटाओ। हमारा मन शिव संकल्प से भरा पूरा हो।” यही बात छह मन्त्रों में दोहराई गई है। सभी मंत्रों की दूसरी पंक्ति में तन्मेमनः शिवसंकल्पमस्तु की टेक है।
गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को मन के निग्रह का उपदेश दिया है। इधर-उधर भागते मन को एक ही विषय पर केन्द्रियभूत करना आसान नहीं है। अर्जुन ने उत्तर दिया, हे कृष्ण मन बड़ा चंचल है। इसे निग्रह करना वायु को हाथ में पकड़ने जैसा कठिन कार्य है। अर्जुन मन की चंचल प्रवृत्ति से व्यथित हैं। उसने श्री कृष्ण का ध्यान खींचा। उत्तर में श्री कृष्ण ने योग के सारभूत तत्व बताए। मन संकल्प का भी केंद्र है। हम अपने दैनिक जीवन में तमाम विचारों से प्रभावित या अप्रभावित होते हैं। हम अपनी प्रकृति को ठीक करने के लिए सत्य और शुभ को ग्रहण करने की शपथ लेते हैं। रात में सोते समय सूर्याेदय के पहले जाग जाने का संकल्प करते हैं। सुबह उठते ही देर हो जाती है और संकल्प धरा रह जाता है। मेरे मन में विचार आता है कि रात में दूसरे दिन सुबह उठने का निश्चय हम ही करते हैं, लेकिन सवेरे उठते समय स्वयं अपना निश्चय काट देते हैं। मन ऐसे ही खेल खेलता है। तमाम सद्कार्यों के लिए हम सब अनुष्ठान करते हैं। संकल्प धराशायी हो जाते हैं। मन जीत जाता है। बुद्धि हार जाती है। भारतीय चिंतन में किसी भी काम को प्रारम्भ करने के लिए प्रगाढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है।
धार्मिक कर्मकांडों में संकल्प की व्यवस्था है। संकल्प मंत्र में दिक् और काल दोनों की आराधना की गई है। यह जम्बूद्वीपे भरतखण्डे से शुरू होता है और आर्यवर्त के बाद कर्मकांड की जगह का उल्लेख होता है। संकल्प मंत्र में समय की बड़ी इकाई से लेकर छोटी सी इकाई का उल्लेख है। संकल्प मंत्र में अस्तित्व के सभी घटकों को सम्बंधित शुभ कार्य से जोड़ा गया है। इनमें दिक्काल के सभी घटक शामिल हैं। यह एक तरह से मन को शुभकार्य से जोड़ने की कार्यवाही है। मनुष्य की पहली परत शरीर है। इसकी दूसरी परत मन है। तीसरी परत बुद्धि है। चौथी परत आत्मा है। मन शरीर के निकट है। बुद्धि के भी निकट है। मन शरीर और बुद्धि दोनों को प्रभावित करता है। शरीर को प्रभावित करने के कारण इसकी शक्ति बड़ी है। बुद्धि पर मन का प्रभाव पड़ता है। हम सब बुद्धिमानी की जगह मनमानी करते है। योग विज्ञान में मन को नियंत्रित करने के अनेक उपाय बताए गये हैं। वैसे मन की अनुकूलता सुख है और प्रतिकूलता में दुःख है। सुख-दुःख की अनुभूति मन के ताल पर ही होती है। मन के प्रभाव में चित्त दशा बनती है। मनोवैज्ञानिक सुख और दुःख दोनों को ही चित्तदशा या स्टेट ऑफ़ माइंड कहते हैं। चित्तदशा की निर्मिति प्रकृति के गहन अध्ययन से भी होती है और प्रकृति सृष्टि के प्रति आस्तिक या नास्तिक भाव के कारण भी होती है।
मन और मनन समीपवर्ती हैं। किसी विषय पर मनन करना समीक्षात्मक भी हो सकता है अथवा आस्था जनित भी। लोक कल्याण के लिए किसी मंत्र को दोहराना भी मनन है। मन के साथ चिंतन भी जुड़ता है। तब इसे चिंतन-मनन कहते हैं। चिंतन-मनन में बुद्धि भी हिस्सा लेती है। भावना प्रधान मन बुद्धि द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को ऊर्जा देते है। भावना की कार्यवाही में सामान्यतः बुद्धि का उपयोग नहीं होता है। तार्किक लोगों में भावना नहीं होती है। मन संकल्प लेकर बुद्धि युक्ति का सहयोग ले सकता है। सामान्यतः शरीर और मन अलग-अलग काम करते हैं, लेकिन मन और शरीर दो नहीं हैं। हमारे व्यक्तित्व का स्थूल हिस्सा शरीर है और अति सूक्ष्म हिस्सा मन है। मन विचलन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। इसी तरह शरीर तल पर होने वाले कष्ट भी मनो क्षेत्र में जाते हैं। प्रसन्न या अप्रसन्न होने का केंद्र भी मन है। मन में होने वाली प्रसन्नता शरीर को ऊर्जावान बनाती है। मन से दुःखी व्यक्ति नियमित दिनचर्या भी ठीक से नहीं कर पाता। इसके विपरीत रोगी शरीर में भी मन की प्रसन्नता दृढ़संकल्प पैदा करती है। हमारी दिनचर्या में बहुत कुछ मनोनुकूल होता है और बहुत कुछ मन के प्रतिकूल। एक विचार है कि हम विपरीत परिस्थितियों का पूरे मन से सामना करें और इच्छित कार्य संपन्न करें। दूसरा विचार भी है। इच्छा शून्य रहे और और मन की किसी कार्यवाही से संघर्ष न करें। अस्तित्व स्वयं खेलता है। उस पर कोई बंधन नहीं।
आशा और निराशा दो नहीं हैं। दोनों मनोभावनाएँ हैं। दोनों का सम्बन्ध मन से है। वस्तुतः दोनों का सम्बन्ध भविष्य काल से है। हम भविष्य में शुभ होने की इच्छा रखते हैं। यह आशा है। लेकिन भविष्य कभी वर्तमान नहीं होता। निराशा का सम्बन्ध भी काल से है। हम भविष्य की तमाम घटनाओं से निराश होते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएँ काल्पनिक होती हैं। भय या डर भी ऐसी ही मनोदशा है। हम अशुभ की कल्पना में भयग्रस्त होते हैं। हमारे शरीर में तमाम रासायनिक परिवर्तन आ जाते हैं।
भय अस्तित्वविहीन है। उससे डरना मन का खेल है। मनुष्य के मन की तरह अस्तित्व का भी एक मन होता है। ऋग्वेद में चन्द्रमा को अस्तित्व का मन कहा गया है- चन्द्रमा मनसो जातः। अस्तित्व से बना मनुष्य मन के प्रभाव में चंचल है। अस्तित्व अखंड सत्ता है। हम सब उसी के हिस्से हैं और मन के अनुसार गतिशील रहते हुए तमाम दुःख-सुख उठाते हैं। सभी प्राणियों का मन गति करता है। मन के निग्रह का अर्थ अस्तित्व के मन से जुड़ जाना भी हो सकता है। योग दर्शन की सारी मान्यताओं का केंद्र मन है। समाधि योग का प्रतिफल है। समाधि वस्तुतः मनविहीन दशा है। अंग्रेजी में उसे माइंडलेसनेस कह सकते हैं। योग की साधनाओं में समाधि का महत्व है। ऋग्वेद के अंतिम सूक्त में मन सामान होने की प्रार्थना है।






