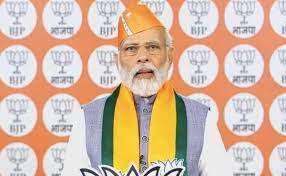-डा. अश्विनी महाजन-
-: ऐजेंसी/सक्षम भारत :-
चौदह दिसंबर 2023 को दुबई में युनाईटेड नेशन फ्रेमवर्क कान्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 28वां सत्र सम्पन्न हुआ, जिसे कॉप-28 के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि कॉप-28 को नतीजों तक पहुंचने में तय सीमा से ज्यादा समय लगा, लेकिन विश्व में इस बाबत खुशी जताई जा रही है कि इस सम्मेलन के बाद दुनिया में मानव जनित ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए बेहतर संभावनाएं होंगी। हालांकि दो सप्ताह तक चलने वाले इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में घोषणाएं की गईं, लेकिन इस सम्मेलन के अंतिम समय में एक ऐसी महत्वपूर्ण घोषणा हुई है, जिससे पूरी दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग और मौसम परिवर्तन से राहत की एक बड़ी उम्मीद जगी है। तेल लॉबी की तीव्र पैरवी के बावजूद, 2050 तक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर सीमित करने के लिए सभी देश जीवाश्म ईंधन, कोयला और तेल एवं गैस दोनों से दूर जाने पर सहमत हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत होने वाले 27 कॉप सम्मेलन इससे पूर्व हो चुके थे, जिनमें कुछ बातें हुई, कहीं-कहीं पर मौसम परिवर्तन और वैश्विक ऊष्णता को थामने के लिए कुछ प्रयास भी हुए, लेकिन विकसित देशों की यह जिद्द कि वे अपनी जीवन पद्धति बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, ने इन प्रयासों के प्रभाव को कम किया। विकसित देशों का यह कहना है कि चाहे जो भी स्थिति हो, वे अपनी जीवन पद्धति को बदल नहीं सकते हैं। सच्चाई यह है कि औद्योगीकरण के समय से लेकर अब तक दुनिया में 23 समृद्ध औद्योगिक देश कुल ऐतिहासिक उत्सर्जन के 50 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार हैं और बाकी 50 प्रतिशत के लिए 150 से अधिक देश जिम्मेदार हैं।
लगभग एक शताब्दी में पेट्रोलियम तेल और गैस का उपयोग 82.34 गुना और कोयले का उपयोग 4.56 गुना बढ़ा है, लेकिन इसमें भी विकसित देशों का योगदान विकासशील देशों की तुलना में कहीं ज्यादा है। हम समझ सकते हैं कि विकसित देशों द्वारा जीवाश्म ईंधनों का उपयोग भी कहीं अधिक अनुपात में बढ़ा है। आधुनिकीकरण और विकास के नाम पर वाहनों के उपयोग में बेतहाशा वृद्धि हुई है। आर्थिक संवृद्धि के और जीडीपी में ग्रोथ के नाम पर औद्योगिक उत्पादन भी भारी मात्रा में बढ़ा है। आज लोग ज्यादा और ज्यादा चीजों का उपभोग करने लगे हैं, जो पूर्व की तुलना में कई सौ गुणा ज्यादा है। वाहनों, उद्योगों, कृषि आदि के परिचालन में पेट्रोलियम पदार्थों सरीखे जीवाश्म ईंधनों का उपयोग बेतहाशा बढ़ा है और इस कारण ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ी है। पिछली एक शताब्दी में वाहनों, विद्युत उत्पादन, औद्योगिक कार्यों और कृषि समेत अनेकानेक गतिविधियों में जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला इत्यादि का उपयोग लगातार बढ़ता गया, जिसके चलते दुनिया में ग्रीन हाऊस गैसों जैसे कार्बनडाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लूरोकार्बन, परफ्लूरोकार्बन व सल्फर हेक्साफ्लोराइड का उत्सर्जन भी बढ़ा। इससे विश्व ग्लोबल वार्मिंग और मौसम परिवर्तन जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। समुद्र स्तर बढऩे के कारण तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपने स्थान से विस्थापित हो रहे हैं, कहीं अल्प वृष्टि तो कहीं अति वृष्टि और तूफानों के कारण दुनिया विभिन्न प्रकार के संकटों का सामना कर रही है। कृषि उत्पादन पर भी संकट आ रहे हैं। कई स्थानों पर तापमान इतना अधिक बढ़ता जा रहा है कि लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। मौसम परिवर्तन पर होने वाले संयुक्त राष्ट्र के तमाम कॉप सम्मेलनों में प्रारंभ से ही यह लक्ष्य रहा है कि दुनिया का तापमान 2050 तक औद्योगएमपीकरण से पूर्व की स्थिति की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा न बढऩे पाए। क्योटो सम्मेलन, जहां ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन की कमी के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, के बाद कॉप सम्मेलनों में बातें तो बहुत हुईं, लेकिन क्योटो सम्मेलन के बाद और कॉप-27 से पहले कोई विशेष प्रगति नहीं दिखाई दी।
जीवाश्म ईंधन से कैसे मिलेगी मुक्ति : हालांकि कॉप-28 में इस बात पर सहमति बनी है कि जीवाश्म ईंधनों के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा, लेकिन इसके लिए अत्यंत गंभीरता से विचार करना होगा कि यह कैसे किया जाएगा।
कॉप-28 में अनेक प्रकार की शपथें ली गई, जिसमें अक्षय ऊर्जा में 3 गुणा वृद्धि, शीतलन से संबंधित ऊर्जा उपभोग में दुगुनी कार्यकुशलता आदि शामिल हैं। पिछले कॉप सम्मेलनों में इस बात पर बहस चलती रही कि जीवाश्म ईंधनों में से कोयले या पेट्रोलियम, किसके उपयोग को कम करना चाहिए। विकसित देशों का यह कहना था कि वे पेट्रोलियम के उपयोग को कम नहीं करेंगे, लेकिन वे साथ ही यह दबाव बना रहे थे कि भारत सरीखे देश कोयले के उपयोग को अवश्य बंद करें। इस बार फिर विकसित देश अंतिम दस्तावेज में शामिल होने में सफल रहे हैं, जब नवीकरणीय ऊर्जा को तीन गुना करने को ‘बेरोकटोक कोयला बिजली को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने’ से जोड़ा गया। हालांकि यह बात मानी जा सकती है कि कोयले से ग्रीन हाऊस गैसों का उत्सर्जन पेट्रोलियम पदार्थों के उत्सर्जन से ज्यादा होता है, लेकिन इस बहस में भारत का यह कहना था कि यदि जीवाश्म ईंधन के उपयोग को क्रमश: कम करना है तो इसमें कोयले और पेट्रोलियम पदार्थों में भेद नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि भारत के पास कोयले के बड़े भंडार हैं, इसलिए भारत के लिए जरूरी है कि फिलहाल वह कोयले का उपयोग कुछ समय तक करे और बाद में उसे क्रमश: घटाया जाए। कॉप-28 के इस फैसले से कि कोयले और पेट्रोलियम में भेद किए बिना सभी प्रकार के जीवाश्म ईंधन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित हो गया है कि इस संबंध में विकसित देशों की बहानेबाजी को कॉप-28 में कम मान्यता मिली।
भारत के पास है ज्यादा समय : हालांकि कॉप-28 में ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित लक्ष्यों, खासतौर पर वैश्विक तापमान को औद्योगिकीकरण से पूर्व की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढऩे दिया जाएगा, की समय सीमा 2050 रखी गई है, लेकिन कॉप-26 में भारत ने अपने वचन में यह कहा था कि हम 2070 तक निवल शून्य (नेट जीरो) के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसलिए भारत के पास वैश्विक लक्ष्य की सीमा से दो दशक आगे का समय रहेगा। हालांकि कॉप-28 में हुई सहमति में चरणबद्ध तरीके से जीवाश्म ईंधनों को समाप्त करने की बात कही गई है, लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि इस लक्ष्य को न्यायोचित्त, व्यवस्थित और न्यायसंगत तरीके से प्राप्त किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अमीर मुल्कों को अपनी जीवन पद्धति को बदलते हुए जिम्मेवारीपूर्वक जीवाश्म ईंधनों के उपयोग को कम करना होगा और भारत समेत विकासशील देशों को इस संबंध में ज्यादा समय मिलेगा।
टिकाऊ उत्पादन ही नहीं, बल्कि टिकाऊ उपभोग भी : अभी तक मौसम परिवर्तन के संबंध में टिकाऊ उत्पादन पर ज्यादा जोर दिया जाता रहा है। लेकिन समझना होगा कि यदि इस पृथ्वी को वास्तव में बचाना है तो संयमित उपभोग से ही ऐसा संभव हो सकता है। अधिकाधिक उपभोग और इस कारण अधिकाधिक ईंधन का उपयोग और प्रकृति का अंधाधुंध शोषण, आज की वैश्विक ऊष्णता का प्रमुख कारण है। सभी देशों की सरकारों को उपभोग को संयमित करने हेतु प्रयास करने होंगे। जी-20 सम्मेलन में भारत ने दुनिया के सामने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है और वह सिद्धांत है-एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और अनुशासन भारत की संस्कृति में ही निहित है। वैश्विक ऊष्णता के संबंध में हमें दुनिया के सामने यह विचार और दृढ़ता से रखना पड़ेगा कि जिम्मेवारीपूर्वक उपभोग से ही इस पृथ्वी को बचाया जा सकता है। सभी देशों के नागरिकों को यह समझना पड़ेगा कि संयमित उपभोग ही ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी के विनाश को रोक सकता है।